गब्बर ने बदल दी हमारी सोच
क्यों पसंद है निगेटिव चरित्र ?
(लेखक अनिरुद्ध जोशी ''शतायु'' सकारात्मक सोच का आईना ब्लॉग पर कभी कभार लिखते हैं, और आप उनको नियमित वेबदुनिया डॉट कॉम पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह इस संस्थान में कार्यरत हैं )
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक 'जज' होता है। जिस व्यक्ति के भीतर जज जितनी ताकत से है वह उतनी ताकत से अच्छे और बुरे के बीच विश्लेषण करेगा। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति स्वयं में सुधार कर भी लेता है जो खुद के भीतर के जज को सम्मान देता है। अच्छाइयाँ इस तरह के लोग ही स्थापित करते हैं।
लेकिन अफसोस की भारतीय फिल्मकारों के भीतर का जज मर चुका है। और उन्होंने भारतीय समाज के मन में बैठे जज को भी लगभग अधमरा कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? और, ऐसा क्यों है कि अब हम जज की अपेक्षा उन निगेटिव चरित्रों को पसंद करते हैं जिन्हें हम तो क्या 11 मुल्कों की पुलिस ढूँढ रही है या जिन पर सरकार ने पूरे 50 हजार का इनाम रखा है और जो अपने ही हमदर्द या सहयोगियों को जोर से चिल्लाकर बोलता है- सुअर के बच्चों!
दरअसल हर आदमी के भीतर बैठा दिया गया है एक गब्बर और एक डॉन। एक गॉडफादर और एक सरकार। अब धूम-वन और टू की पैदाइश बाइक पर धूम मचाकर शहर भर में कोहराम और कोलाहल करने लगी है। शराब के नशे में धुत्त ये सभी शहर की लड़की और यातायात नियमों के साथ खिलड़वाड़ करने लगे हैं।
वह दौर गया जबकि गाइड के देवानंदों और संगम के राजकुमारों में बलिदान की भावना हुआ करती थी। 60 और 70 के दशक में नायक प्रधान फिल्मों ने साहित्य और समाज को सभ्य और ज्यादा बौद्धिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जबकि रूस से हमारे सम्बंध मधुर हुआ करते थे और साम्यवाद की सोच पकने लगी थी, लेकिन इसके परिणाम आना बाकी थे।
लेकिन जब आया गब्बर, तो उसने आकर बदल दी हमारी समूची सोच। शोले आज भी जिंदा है जय और विरू के कारण नहीं, ठाकुर के कारण भी नहीं गब्बर के कारण।
सुनने से ज्यादा हम बोलना चाहते हैं और 90 फीसदी मन निर्मित होता है देखने से ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। जब हम सोते हैं तब भी स्वप्न रूप में देखना जारी रहता है। मन पर दृष्यों से बहुद गहरा असर पढ़ता है। दृश्यों के साथ यदि दमदार शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सीधे अवचेतन में घुसती है बात। इसीलिए आज तक बच्चे-बच्चे को 'गब्बर सिंह' के डॉयलाग याद है। याद है 'डॉन' की अदा और डॉयलाग डिलेवरी।
भाषा और दृश्य से बाहर दुनिया नहीं होती। दुनिया के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे फिल्मकारों को यह बात कब समझ में आएगी की वह जो बना रहे हैं वह देश के वर्तमान के साथ खिलवाड़ करते हुए एक बहुत ही भयावह भविष्य निर्मित कर रहे हैं, यह जानते हुए कि हमारा मुल्क भावनाओं में ज्यादा जीता और मरता है।
शोले से जंजीर, जंजीर से डॉन, खलनायक, कंपनी और फिर एसिड फैक्ट्री तक आते-आते हमारी सोच और पसंद को शिफ्ट किया गया। यह शिफ्टिंग जानबूझकर की गई ऐसा नहीं है और ना ही अनजाने में हुई ऐसा भी नहीं। छोटी सोच और बाजारवाद के चलते हुई है यह शिफ्टिंग। अब हमें पसंद नहीं वह सारे किरदार जो प्रेम में मर जाते थे अब पसंद है वह किरदार जो अपने प्रेम को छीन लेते हैं। प्रेमिका की हत्या कर देते हैं और फिर जेल में पागलों से जीवन बीताकर पछताते हैं।
फिल्मकार निश्चित ही यह कहकर बचते रहे हैं कि जो समाज में है वही हम दिखाते हैं। दरअसल वह एक जिम्मेदार शिक्षक नहीं एक गैर जिम्मेदार व्यापारी हैं। यह कहना गलत है कि फिल्में समाज का आइना होती है। साहित्य समाज का आईना होता हैं। क्या दुरदर्शन पर कभी आता था 'स्वाभीमान' हमारे समाज का आईना है? एकता कपूर की बकवास क्या हमारे समाज का आईना है? आप खुद सोचें क्या 'सच का सामना' हमारे समाज का सच है?.

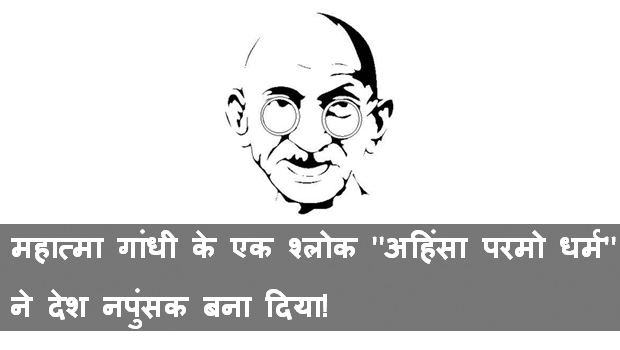
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
हार्दिक निवेदन। अगर आपको लगता है कि इस पोस्ट को किसी और के साथ सांझा किया जा सकता है, तो आप यह कदम अवश्य उठाएं। मैं आपका सदैव ऋणि रहूंगा। बहुत बहुत आभार।